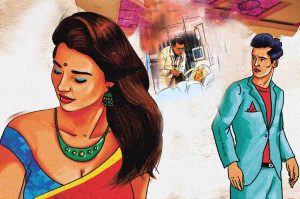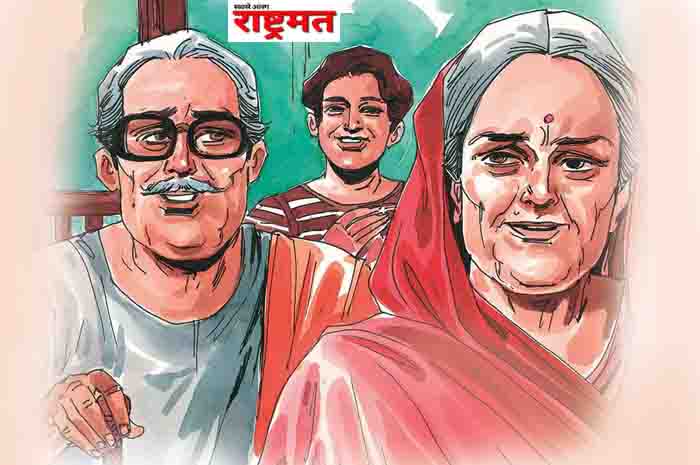
LAST STOP
तकलीफ तन्हाई की क्या होती है, बुजुर्ग माता पिता ही जानते हैं। जिनके बेटा- बहू वृद्धाआश्रम में उन्हें छोड़ जाते हैं। अथवा अपने बेटा बहू की वजह से उन्हें ‘ओल्ड होम’ में आना पड़ता है। बुढ़ाते अभिभावकों की देखभाल की जद्दोजहद से परिवारों में संकट बढ़ रहे है। जिनके समाधान खोजे जा रहे है। डॉ. आरती स्मित इसी विषय पर कहानी लिखी हैं ‘अंतिम पड़ाव’
तीन कविता संग्रह, दो कहानी संग्रह, दो बाल साहित्य, दो आलोचना संग्रह, 40 से अधिक पुस्तक अनुवाद, धारावाहिक ध्वनि रूपक एवं नाटक, रंगमंच नाटक लेखन, 20 से अधिक चुनिंदा पुस्तकों में संकलित रचनाएँ, बतौर रेडियो नाटक कलाकार कई नाटकों में भूमिका. विभिन्न उच्चस्तरीय पत्रिकाओं में सतत लेखन. सत्यवती कॉलेज,दिल्ली में अध्यापन.
अंतिम पड़ाव
“लो, खाना खा लो|”
“तुसी खा आए?”
“हम्म! वहीं खा लिया| दो-दो प्लेटें लाने में दिक्कत होती न!|”
“हम्म! आज ठंड कित्ती जबरदस्त है!”
“हाँ, तुम कंबल से न निकलो| मैं बेड के पास ही टेबल लगा देता हूँ|”
“क्या-क्या करोगे मेरे लिए? तुम ही कौन-से जवान हो!”
“ओय, मैनूँ बुड्ढा न कह| अब भी फिट हूँ| बिना लिफ्ट के नीचे आ-जा सकता हूँ|” उसने पत्नी को हँसाने की कोशिश की| पति की कोशिश को नीलू ने जाया न होने दिया| मुस्कुरा दी तो उसका चेहरा खिला गुलाब हो गया|
“आज कामिनी नहीं आई?”
“नहीं! उसे बुखार हो गया है| सुबे फोन किया था उसने, तो कह रही थी, ‘अंकल जी बुखार उतरते ही आ जाऊँगी’| मैंने ही कहा, ‘कल भर आराम कर ले| मैनूँ करना इ की है| पका-पकाया खाना मिलदा है, खाना है और लाना है| कमरे में इक दिन साफी नइ लगेगी तो कोई भूचाल थोड़ी न आ जाएगा’|”
टेबल को बिस्तर की तरफ़ खिसकाते हुए उसने कहा| फिर, थरमस से गुनगुना पानी गिलास में आधा भरने तक उड़ेला। थरमस का मुँह अच्छी तरह बंद कर आले पर रख दिया और गिलास टेबल पर रखते हुए वह पत्नी की बगल में जा बैठा| चंद मिनट भी न बीते कि सिराहने तकिया लगाकर, पाँव सीधा करते हुए वह कंबल में गुडुप गया|
“अभी तो जवान बन रहे थे| अब क्या हुआ?” नीलू मुँह में निवाला डालती हुई बोली| उसके चेहरे पर मसखरी की छिटकती चाँदनी देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा|
“ओय,क्या जवानों को ठंड नी लगदी?”
“लगदी है, लगदी है|” हँसी दबाती हुई वह खाना ख़त्म करने में जुट गई|
‘देखते-देखते महीना बीत गया| नीलू अब यहाँ के माहौल में एडजस्ट करने लगी है| वैसे भी उसने जाना कहाँ है, इसी फ्लोर पर चार कदम चल ले, यही बहुत है| वॉकर मँगा तो दूँ, मगर लेकर चले तो न! छड़ी तक तो पकड़ना नइ चाहती| पर अब तो उसे समझना होगा कि घुटना ज़िद पे अड़ा है| वॉकर न सही, सेफ़्टी के लिए छड़ी तो पकड़नी ही पड़ेगी |’ उसने करवट बदली|
नीलू अब भी खा रही थी| एक-एक निवाला देर तक चबाती-चुभलाती हुई| इत्मीनान से| कोई जल्दबाजी नहीं| सोच के पंख खुलने-फड़फड़ाने लगे तो उसने लंबी साँस भरकर उन्हें उड़ान भरने की इजाज़त दे दी| मुँह में जाता एक-एक निवाला सोच को गति देता जाता|
‘अज़ीब बात है, मुफ़्त में खिलाए जा रहे ये निवाले अब एहसान भरे नहीं लगते| इन निवालों में किसी की बड़बड़ाहट, गुस्सा या बद्दुआ शामिल नहीं है| जो भी लोग यहाँ ढेर सारे राशन या बाकी चीज़ें दे जाते हैं, उनमें समर्पण का भाव होता है, दया का नहीं| और जो भोजन का आयोजन करते हैं, उनकी श्रद्धा देखकर तो आँखें भर आती हैं| बूढ़ों के लिए कित्ती इज्ज़त है उनके मन में! क्या वे घर के बूढ़ों के साथ भी ऐसे ही रहते होंगे — प्यार और सम्मान से भरे-भरे? या फिर…’ सोच को आगे धकियाती-गिराती हुई वह जल्दी-जल्दी अंतिम कौर चबाने लगी|
“टीवी चला दूँ?”
“नहीं!”
“अचानक क्या सोचने लगी?” पत्नी को कंधे तक कंबल ओढ़ाते हुए उसने पूछा|
“नहीं, कुछ ख़ास नहीं|”
“फिर भी, कुछ तो… जानती हो न, बिना देखे भी तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकता हूँ|”
“सोच रही हूँ, बाबाजी ने जितना अच्छा जीवनसाथी दिया, उतने अच्छे न सही, मगर ऐसे बच्चे तो देते जिन्हें हम बोझ न लगते|”
“छोड़ न! हमने अपना करम किया, वे जो ठीक समझ रहे हैं, कर रहे हैं|”
“यहाँ हर रोज़ कोई न कोई आता-मिलता है और कितने प्यार से भेंट दे जाता है!”
“तभी तो किचन में ख़ुशबू बरकरार है| चाय, नाश्ता, दूध, भोजन सब समय पर बिना किसी किटकिट, बिना हील-हुज्जत के| अपने को और क्या चाहिए!”
“वह भी बिना पाई खर्च हुए| मगर मेरा सवाल दूसरा है?”
“कि पाई भर का भी खर्च क्यों नहीं है? भई अब पाई मिलती कहाँ है, खर्च होगा तो कम से कम एक रुपया|” उसने ठिठोली की|
“तुम्हें तो बस मसखरी सूझती है|”
“नीलू! मुद्दत बाद हँसने का मौका मिला है तो बीते कल की गठरी उठाए ख़ुद को क्यों रुलाना?” वह गंभीर हो गया|
“नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था| मुझे बस ये ख़याल आया कि जो लोग यहाँ हमलोगों से इत्ते प्यार से मिलते हैं, वे लोग तो अपने घर के बड़े-बूढ़ों को पूरी इज्ज़त देते होंगे न?”
“यह ख़याल नहीं, एक ऐसा सवाल है, जिसका कोई निश्चित और पुख्ता ज़वाब नहीं| हर घर की धूप-हवा अलग होती है| बाहर से झाँककर उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता|”
“हम्म! कई बार तो घर के भीतर रहकर भी कमरे अपनी-अपनी दीवारों के कान खुले मगर जुबां बंद रखते हैं| ऐसा न होता तो … वह चुप हो गई| आँखें बंद ली|
यह संकेत था,संवाद रोक दिए जाने का| अभी तक चुलबुलाते उस कमरे की हवा में अचानक भारीपन आ गया| गहरी उसाँसें भीतर के गुबार बाहर निकाल फेंकने को मचलतीं, दिमाग ठहाके लगाता, मज़ाक उड़ाता –- क्यों मि. इंदर! कैसा लग रहा है?
‘उँह, अच्छा! बहुत अच्छा| आख़िर इस कमरे का मालिक तो मैं हूँ| कोई मुझे निकाल-बाहर करने की हिम्मत नहीं कर सकता| जब ख़ुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली तो अब किस बात का रोना| दिल्ली का घर बेचते समय कब सोचा था, दिल्ली वापस बुला लेगी और वापसी भी इस रूप में होगी! जिस शहर के चप्पे-चप्पे में मेरे बचपन की यादें शामिल हों, जवानी की मस्ती नहीं, ज़िम्मेदारियाँ शामिल हों और फिर भी मुस्कुराता बसंत अपने नाम हो, उसी शहर में इस तरह वापसी … अपने घर से बेदख़ल होकर… नहीं… विस्थापित होकर… लुटे-पिटे से … ओह!’
उसने माथे पर पड़े बल को हथेलियों से सहलाया|
‘नहीं! हम लुटे-पिटे नहीं हैं| चंदर ने हमें बेघर नहीं होने दिया| सारी ज़रूरी सुविधाएँ जुटा दीं| उन नामुरादों के गाल पर क्या ये कम बड़ा तमाचा है! हह! बड़ा गर्व था हमें, अफ़सराना ठाठ भोगते हम, बेटों को भरते समय सोच ही न सके कि रिटायरमेंट के बाद जीना मुहाल हो जाएगा| नीलू तो जैसे चोट खाते-खाते जड़ हो चली है| आज इसे देखकर भला कौन कहेगा, यह अपने दफ़्तर की एक्टिव और बेस्ट डिसीजनमेकर मानी जाती होगी! एक गलत निर्णय ने हमें यहाँ पहुँचा दिया| लेकिन, क्या हमारा निर्णय सचमुच गलत था? बेटे-बहू को पूँजी सौंपकर एक साथ रहने की इच्छा रखना क्या सचमुच बेवकूफ़ी है?’
उसे लगा, पलकें छलके खारे पानी से भीगने लगी हैं तो हौले से उँगली फिरा दी| आँखों के आगे वे गर्वीले पल नाच उठे जब पहली बार पिता बना था|
‘विवेक रूप-रंग में बिलकुल नीलू जैसा दिखता तो वह इठलाकर कहती, माँ की शक्ल का बच्चा बड़ा आज्ञाकारी होता है| विवेक नाम भी तो उसी ने रखा था| विवेक आज्ञाकारी तो है, मगर बुरी आदतों ने उसकी ज़िंदगी के उठान को ग्रस लिया|सच ही है, कभी-कभी बहुत सुख-सुविधा बच्चों की बरबादी का कारण बनती है|’
उसने ज़ोर लगाकर फेफड़े में साँस भरी|
‘विवेक जैसा भी है, हमारे कहे की इज्ज़त तो करता ही है| उसने समय और हमारे दिए पैसे की कद्र की होती तो आज की तारीख़ हमारी ज़िंदगी को कुछ अलग हर्फ़ों में लिखती| कहीं न कहीं उसे भी मलाल है तभी तो हमारी ज़रा-सी बीमारी सुनकर भागा आता है| पाँच-छह घंटे का सफ़र कोई कम थोड़ी न होता है|’ उसने मन को समझाया|
‘और इलू भी तो मिलने आई ही| पोती को सामने पाकर नीलू तो फिर जी उठी थी| अब तक इस जगह को वह अपना नहीं मान पाई है| रह-रहकर भूल जाती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में अब यही हमारा ठिकाना है| जब-तब घर जाने की ज़िद करती है| उसे कैसे समझाऊँ कि बेटे को पूँजी सौंपकर हमने मकान तो बना लिया पर उसके भीतर हमारा घर खो गया| उस बड़े आरामदेह मकान में हम दोनों के लिए कोई कोना घर न बन सका| रिटायरमेंट के बाद भाग-दौड़ से निज़ात पाकर उस पहाड़ी मकान में सुस्ताने और पोते-पोतियों के साथ फिर से बचपन जीने की ललक में हम ये तो भूल ही गए कि हमारा सुस्ताना भला औरों को क्यों अच्छा लगेगा! उस पर, बुढ़ापे की बिन बुलाई सखियाँ! कोई अपना ढेर सारा समय बुड्ढों को क्यों दें भई, बच्चों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है| नितेश कहाँ तक समझा पाता पत्नी को! सरला को भी गलत कैसे कहूँ! मकान के लिए पैसे दिए थे, अपनी सेवा के लिए थोड़ी न, जो कोई दावा करें| मकान है, रहो और अपनी देखभाल ख़ुद करो|’
वह अपनी ही सोच पर मुस्कुराया| ‘ख़ुद पर व्यंग्य कसना भी एक अनुभव ही है| नीलू जॉब पर निकल जाती थी तब माँ को भी ऐसा ही लगता होगा न! अपनी देखभाल ख़ुद करने की विवशता से वह भी भरी-भरी रहती होगी, तभी तो दस दिन में वापस चंदर के पास जाने की ज़िद करने लगती थी| उनके यहाँ आने पर हम ही उनकी कौन-सी सेवा कर पाते थे! जॉब ही ऐसी थी| सुबह आठ बजे निकलो और शाम सात बजे लौटो| फिर बच्चों की फ़रमाइश सुनो| डिनर साथ लेने के सिवा माँ के साथ समय ही कितना बिता पाते थे! और छुट्टी का दिन तो बस कामों का ज़खीरा उठाए होता| शीलू और चंदर की जॉब इतने लंबे समय की नहीं थी, शायद इसलिए माँ को उनका समय मिलता रहा हो और दोनों पोतियाँ भी आसपास डोलती रहती होंगी! विवेक और नितेश तो ठहरे उत्पाती लड़के, दादी को घेरकर कहाँ बैठते होंगे!… मगर नितेश की बीबी सरला तो जॉब नहीं करती| घर पर ही होना होता है उसे| यह तो मानना पड़ेगा, चंदर और शीलू ने सारे रिश्ते बड़े प्यार और सम्मान से निभाए, वरना अपने बेटे-बहू अपने नहीं होते, देवरानी-जेठानी की बात ही क्या! तक़दीर भी क्या निराली चीज़ है! कब सोचा था जिन बच्चों की उँगली पकड़कर स्कूल बस में बिठाने जाते हैं, एक दिन एक तो हाथ ही छुड़ा लेगा, दूजा उँगली पकड़कर यहाँ पहुँचा जाएगा| विवेक की चुप्पी और नितेश के झुके सिर बहुत कुछ कहते हैं, पर क्या करें! सब समझता हूँ, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं|’
उसने करवट बदली| पत्नी की तरफ़ मुँह उठाकर देखा तो वह कहीं दूर जाकर ठिठकी-सी लगी, जहाँ तक उसकी आवाज़ भी न पहुँच पाए| ‘शायद अतीत की धुँध से घिरी है| शायद, घर का बार-बार बनना-बिखरना और जीवन का यों ही रिक्त होते जाना परेशान किए हुए है| नितेश उसका लाडला! अपनी पत्नी को समझा न सका कि मकान साझा खरीदा तो मालिक वे दोनों कैसे हो गए| जिस घर में छोटा मुखिया बन जाए, उस घर के बड़ों के समझौते के दिन शुरू हो जाते हैं| बेटा बाप हो जाता है, ज़िम्मेदारी लेने में नहीं, ख़र्च कटौती करने में| बेबे-बापू के हिस्से के जायज ख़र्च भी फ़िज़ूल लगने लगते हैं| तभी तो नीलू को एक्सीडेंट के बाद किसी बड़े डॉक्टर से दिखाने की बात पर सरला नितेश पर चढ़ बैठी| मैं तो नाप ही नहीं पा रहा था कि नीलू किस दर्द से अधिक बेचैन है, पाँव की हड्डी टूटने से या सरला की जुबान से झड़ते ज़हर से! उस ज़हर ने आख़िर पुरानी नीलू को अचेत कर ही दिया| ये तो कोई और लगती है| चलती-फिरती उसकी डमी, जिसके भीतर फीड की गई यादें रह-रहकर उत्पात मचाती हैं|
काश, मैंने चंदर का कहा माना होता! हम दोनों को उसकी सलाह चुभती रही| थककर उसने समझाना छोड़ दिया, मगर हमारी ज़िम्मेदारी ओढ़ ली| वे लोग भी तो रिटायर्ड हैं| एक वह वक़्त था जब हमें दो बेटों के माँ-बाप होने का गर्व और चंदर-शीलू के दो बेटियाँ होने पर अफ़सोस होता था| नीलू ने हँसी-हँसी में कहा भी था – ”बेटियाँ तो छोड़कर चली जाएँगी, अपने ये दोनों मुंडे ही तेरे काम आएँगे| इन्हें अपना बनाकर रह|”
तब, शीलू से पहले चंदर ने तपाक से ज़वाब दिया था—“सारे अपने ही हैं जी, इसमें बनाना क्या! ये तो संस्कार की बात है| बेटियों को दर्द होगा तो वे भी भागी-भागी आएँगी|”
चंदर का कहा सच हुआ| वक़्त ने हमारे मुँह पर ताला जड़ दिया है| जिस तरह बार-बार मौत के मुँह से वे दोनों निकाले गए हैं, जिस तरह बेहतर से बेहतर इलाज की संभावना बनी, बेटियाँ तो बेटियाँ, रिश्तेदार, मित्र—सभी सेवा और सहयोग के लिए एकजुट खड़े रहे, यही तो चंदर-शीलू की असली कमाई है| माँ का आशीर्वाद भी तो उन दोनों के साथ है| बेटियों ने उनसे घर जोड़े रखने और बड़ों की सेवा का संस्कार पाया है| उसने बेटियों पर धन नहीं लुटाया, उन्हें इस लायक बनाया कि वे उससे अधिक धन कमा सकें और अपने व्यवहार से ससुराल में भी सबका दिल जीतें, यश कमाएँ| वे दोनों बेटियों की बैसाखी नहीं बने| हमने यहीं गलती की, बार-बार की| अब जीवन के चौथे पहर में पछताकर भी क्या होना है! अपनी-अपनी किस्मत!’
उसने आँखें बंद कर लीं| नीलू तकिए के सहारे बैठी ही रही| मौन का एक अभेद्य घेरा उसके चारों ओर बड़ी मज़बूती से जड़ा था| उसने चाहा, पत्नी को टोके, मगर फिर उस घेरे को तोड़ने की चाह छोड़ दी|
’नीलू यहाँ,मेरे पास होकर भी कहीं दूर यात्रा पर है| यादों के थपेड़े उसे चैन लेने नहीं देते| बड़े पद का रूआब, बड़ी बहू होने और एक समय के बाद ससुराल की बँधी-बँधाई ज़िम्मेदारी से लगभग मुक्त रहनेवाली नीलू अपने ही घर से बेघर होना, परिवार से टूटना,टूटकर यहाँ आने की नियति को अब तक स्वीकार नहीं पाई है|…या अपनी जगह सरला को रखकर देख रही है कि किसके वक़्त का पलड़ा अधिक भारी है|’
उसने आँखों पर रखा हाथ बदला| सोच की गली के भीतर की गली में घुसता हुआ आगे बढ़ता रहा| ‘बाबूजी के जाने के बाद दादाजी ने हिम्मत न रखी होती और माँ ने धैर्य और संयम नहीं साधा होता तो क्या हम इस तरह पाले जा सकते थे? दादाजी ने अपने दोनों बेटों के परिवार को समान समझा, मगर पोते का फ़र्ज़ निभाया सिर्फ़ चंदर ने | मैंने बसंत आने से पहले शिशिर ओढ़ लिया; बड़े बेटे और भाई का फ़र्ज़ पूरा करने में कोर-कसर न छोड़ी| अभाव की सुलगती लकड़ी के बीच बिन बाप का बड़ा बेटा होना घर का मुखिया होना ही नहीं होता है, फ़र्ज़ की चलती-फिरती दुकान होना भी होता है| मेरे वे एहसास सिर्फ़ मेरे हैं| उसे हूबहू कोई नहीं समझ सकता| चंदर भी नहीं| माँ समझती रही होगी, तभी उनके चेहरे पर हम दोनों को लेकर कभी सिलवटें नहीं आईं| उनका ही आशीर्वाद रहा कि हम दोनों अच्छी नौकरी पा गए और हमारी गृहस्थी ने किसी बेटे को अभाव का कील चुभने नहीं दिया| बहू भी बड़े प्यार से लाए, फिर कहाँ चूक हो गई?’
मुँदी पलकों तले जागती आँखों में जाने कितने सवाल उमड़ पड़े थे! वह जितना सोचता, उतना ही विचारों के खोह में खोता जाता| ‘अगर चंदर और शीलू ने आदर-सम्मान न दिया होता तो वे इतने संतुष्ट न होते| खैर, माँ ने भी पोतियों पर पूरा प्यार लुटाया ही| उन दोनों की अनुपस्थिति में बच्चों के लिए घर को घर जैसा बनाए रखा, ताला बंद मकान कभी न बना, जबकि हम दोनों के नौकरी पर जाने के बाद बच्चे स्कूल से लौटते तो घर पर उनके सिर सहलाकर पूछने वाला कोई न होता कि आज दिन कैसा गुज़रा| कमाना हमारी मज़बूरी थी| मैं नहीं चाहता था, मेरे बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में कोई कमी रहे, मगर उस मज़बूरी ने हमारे आपसी डोर को मज़बूत न होने दिया| उनके किशोर मन को समझने का वक़्त न मिला; शरीर और मन में होनेवाले बदलावों पर कभी बिठाकर चर्चा नहीं की, न सही-गलत समझाया| शायद, इसलिए वे मेधावी होकर भी भटक गए| विवेक बुरी संगत में न पड़ा होता तो आज मनचाहे मुक़ाम पर होता| उसे संभालने में हमने देर कर दी| आज दोनों भाई अपनी-अपनी ज़िंदगी के कई पड़ाव पार करने के बाद भी वह मंज़िल नहीं पा सके जो उनके खोए पलों की क्षति पूरी कर दे|
…ओह! क्या-क्या सोचने लगा हूँ! क्या होगा सोचकर? क्या ये अच्छा नहीं कि वे अपनी ज़िंदगी ठीक से जिएँ, अपने बच्चों को सही ढंग से पालें? हम भी तो हमउम्रों के बीच हैं| और कोई काम भी नहीं, न किसी पर बोझ बनने का दबाव ही है| वानप्रस्थ आश्रम का आधुनिक और बेहतर रूप| फर्क़ इतना है कि पहले अपने आपको गृहस्थ जीवन से निकालकर ईश्वर-चिंतन के लिए वन जाते थे और प्रकृति की गोद में आश्रम बनाकर रहते हुए सादा-सरल जीवन बिताते थे| अब तो कई जगह वनवासियों को ही वन से खदेड़ा जाता है| जो सदियों से जितने टुकड़े पर पैर टिकाए हैं, तो हैं, शेष वन वन विभाग का| वहाँ भी व्यापार और कई क़ारोबार| अब तो हरे-भरे पहाड़ तक बेचे जा रहे हैं और उन पहाड़ों से उनकी हरियाली छीनकर उन्हें सख्त पत्थरों में तब्दील किया जा रहा है| शांति और साधना के लिए वनवास आकाशकुसुम की तरह है| और हम भी कहाँ के साधक! तीनों समय भोजन और तेज़ धूप,बारिश से बचने की चाह रखनेवाले आरामपसंद आधुनिक शहरी बूढ़े! चाहते हैं कि ज़ेब इतनी तो गर्म हो कि बिन बुलाए मेहमान की तरह आई बीमारियों से लड़ा जा सके और अपनी सेवा-टहल के लिए किसी सेवक को भी रख सकें| कोई माने न माने, अब यह हमारी ज़रूरत बन चुकी है| प्रकृति से निकटता का अर्थ बदलता जा रहा है| यों भी वक़्त कब किस करवट बैठे, यही तो पता नहीं होता| चंबा में मकान बनाते समय कब सोचा था, प्रकृति से दूर कांक्रीट के जंगल में फिर आना पड़ेगा और यहीं हमारा आख़िरी आशियाना होगा! यहीं, इसी शहर में जहाँ जीवन ने ही नहीं, घर ने भी तीन बार रूप बदला| इसी को कहते हैं, “लौट के बुद्धू घर को आए|”
घर! सब कुछ होने के बाद भी इसको घर क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कह पाते? कितना अच्छा हो, इसका नाम आश्रम या आवास की जगह ‘घर’ कहें|‘घर’ का कोई विकल्प नहीं है, चाहे इस शब्द को जितने विकल्प सौंपे जाएँ| क्यों न कोई अच्छा नाम सोचा जाए!’
उसे अच्छा लगा| सोचों ने ख़ुद ही दिशा बदल ली तो वह मुस्कुराया| उसने मुँदी पलकें खोल दीं| नीलू डायरी में कुछ लिखने में तल्लीन थी| उसने मोबाइल उठाकर समय देखा| ‘चार बजने वाले हैं,लक्ष्मण चाय लेकर आता ही होगा|’ वह उठ बैठा और तकिये को पीठ के पीछे लगाकर उसके सहारे टिक गया|
“तुम लेटी नहीं? लंच के बाद से बैठी ही हो?”
“हम्म! दिल नहीं किया| यहाँ थकान ही क्या होती है जो नींद आए| वह कविता सुनी है तुमने…. बेफिक्री की नींद वाली….?”
“हम्म, पर ठीक से याद नहीं|”
“पंक्तियों के भाव बिलकुल हमारे जीवन का सच लिए है| जब भागमभाग होती है, तब आराम की इच्छा होती है; लगता है, कब सारे झंझटों से छुटकारा मिले, मगर सब सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाती हैं, तब शरीर तो आराम चाहता है, मगर मन अपनों का साथ चाहता है| और देखो, तब नई पीढ़ी उसी भागमभाग में फँसी रहती है और हमारा समय काटे नहीं कटता| चौबीस घंटे चौबीस दिन जित्ते लंबे लगते हैं| कई बार तो एक-एक मिनट बिताना ताड़ के पेड़ पर चढ़ने जैसा लगता है| दिल करता है, मेरी रूटीन कविता की उन पंक्तियों की तरह हो जाए—फिर से टिकटिक दौड़ें टाँगे /और मैं सो जाऊँ ज़िम्मेदारी ओढ़-बिछाकर … ‘ “
“सही कहा| मुझे भी वह कविता बहुत पसंद है| क्या तो भला –सा शीर्षक है …”
“एक पूरी नींद”
हाँ,वही| जब पढ़ा था,तब जानता नहीं था कि इसे लिखने वाले ने तब जीवन के पाँचवें बसंत को भी नहीं छुआ था| फिर भी, हम बुड्ढों के मन को इतनी अच्छी तरह समझ लिया| हम अस्सी-सौ वालों के दिलो-दिमाग को पढ़ना इतना आसान तो नहीं!”
“रब दी नेमत है| और क्या!”
“वो तो है …..”
“इंदरजी! इंदरजी….कमरे में हो क्या?”
कुंडी खड़की और साथ ही ग्रोवर साहब की आवाज़ भी घुस आई| अपनी बात अधूरी छोड़ वह दरवाज़े की तरफ़ देखने लगा|
“आओ जी आओ, ग्रोवर साहब! दरवाजा खुला है|” उठकर सीधे बैठते हुए उसने ज़वाब दिया और बिस्तर से उतरने लगा|
–
यहाँ आते ही वह जान गया था, चुस्त-दुरूस्त, अभिनेता देवानंद-से हैंडसम, चेहरे पर नूरानी चमक लिए मुस्कुराते हुए, सबकी खैर-ख़बर पूछते और मदद को डोलते, जीवन की एक सौ एक पारी खेल चुके ग्रोवर साहब इस आवास के दूसरे सबसे पुराने निवासी हैं और उम्र में भी सबसे बड़े हैं| उसने उनके चेहरे पर कभी हताशा या निराशा नहीं देखी; कभी किसी की बुराई करते नहीं सुना| उनके बेटे भी उन पर जान छिड़कते हैं| बेटे क्या,पूरा परिवार ही … फिर वे यहाँ क्यों आए होंगे, यह सवाल रह-रहकर सिर उठाता रहा, मगर पूछ न सका| ऐसा नहीं था कि पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी | दरअसल, उनके सामने आते ही एक पॉजिटिव औरा चारों और फैलता हुआ अपने आगोश में भर लेता, फिर किस कमबख़्त को याद रहे कि क्या पाया, क्या खोया! उस समय तो उनसे बात करने का अपना ही आनंद होता है| उनके उसी औरा की दमक में हर बार यह सवाल कहीं खो जाता| नीलू उनके कमरे तक जा नहीं पाती और उसे अकेले छोड़कर वह, तो उन दोनों को उनके साथ का सुख कम ही मिल पाया| आज ग्रोवर साहब ख़ुद चलकर आए है, सोच-सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई|
“क्यों भई, सब खैरियत?” कुरसी पर बैठते हुए ग्रोवर साहब पूछ बैठे| उनका केयर टेकर उनके पास खड़ा रहा|
“हाँ प्रा’जी! सब खैरियत है| वो नीलू के पाँव में तकलीफ ज़रा बढ़ गई थी तो उसे अकेले छोड़कर आपसे मिलने जा नइ पाया|”
“ओय, कोई नी जी! आप नी आ सके, असि आ गया| मैनूं बड़े दिनों से आप दोनों नी दिखे तो सोचा,मिल आवां|”
“प्रा’जी! मैं परसों सुबे गिर गई थी तो…”
“मोच-वोच तो नी आई? डॉक्टर के पास चलें?”
“नइ-नइ प्रा’जी, दवा ला दी है| अब दर्द में आराम है|”
“ओय इंदर जी! यार टाला न करो|” फिर जाने क्या सूझी, मुस्कुराने लगे, फिर बोले,
“पहले मैं भी ऐसा ही था| मगर अब पहले वाली गलतियाँ नहीं करता कि दर्द दबाए बैठा रहूँ| मेरे कारण मेरे दलजीते नूं बड़ी परेशानी हुई| केस तो बिगड़ ही गया था, समझो| एक नहीं, दो-दो बार मौत को धक्का देकर मुंडा मैनूं वापिस ले आया| रब सबको ऐसा पुत्तर और परिवार दे| इस बुड्ढे के लिए सब एक दिन-रात एक कर देते हैं….”
बोलते बोलते ग्रोवर साहब अचानक चुप हो गए| शायद, नीलू का चेहरा पढ़ लिया उन्होंने, इसलिए बात बदलते हुए बोले, “अबी चलता हूँ| कोई काम हो तो बताना| मेरा फोन नंबर है कि नी?”
“है जी! चंदर ने दिया था|”
“इसका भी रख लो|” उन्होंने अपने केयर टेकर की तरफ़ इशारा किया|
“और कोई काम, कोई ज़रूरत हो, तो बोलने में शरम मत करना| यहाँ किसी को कुछ होता है, मुझे ही बुलाते हैं| बड़ा हूँ न सबसे, तो सब गार्जियन बनाए हुए हैं|”
“आपके बारे में सब बहुत तारीफ़ करते हैं|”
“ओ जी, मैं क्या, सब रब कर दित्ता है| मैं तो एविं नाम कमा रहा| और क्या! अच्छा बहन जी! अब आदेश दो| और ज्यादा सोचा ना करो| रब जो करता है, भले के लिए करता है|”
ग्रोवर साहब ने आदतन हाथ जोड़े और कुर्सी से उठ खड़े हुए| केयर टेकर पीछे-पीछे चला| ग्रोवर साहब लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों की तरफ़ बढ़े, फिर रुके और सुषमा जी हाल लेने उनके दरवाजे पर जा खड़े हुए और कुंडी खड़काई|
वह अपने दरवाज़े पर खड़ा सोचता रहा, ‘इस उम्र में भी ख़ुद जा-जाकर हाल पूछने वाला यह बंदा सचमुच रब का बंदा है!’ फिर कमरे में आ गया| लक्ष्मण चाय लेकर आ गया था|
“सुषमाजी के कमरे से ठहाके की आवाज़ आ रही है| कोई आया लगता है|”
चाय का खाली कप रखती हुई नीलू बुदबुदाई|
“हम्म! आया होगा कोई रिश्तेदार या …!”
“न, रिश्तेदार नहीं| ऐसी जगहों पर रिश्तेदार आते भी हैं तो हँसी का टोकरा बाहर ही छोड़ आते हैं| हँसी-ठहाके पर मानो रोक लगी हो|”
“अपना तो कोई नी आने वाला| मज़े ही मज़े हैं| एक चंदर था तो आकर मिल गया| अब तो वह भी सात समंदर पार बैठा है| उसके गए हुए भी दो महीने हो गए| दिल्ली की ठंड जैसी, गरमी उससे दो क़दम आगे …. बिजली न रहे तो शरीर में फफोले हो जाएँ| समय कितनी जल्दी बीत गया| है न?”
“हम्म! पाँच महीने हो गए| मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि हमें यहीं रहना है| अब यही हमारा …” नीलू चुप हो गई| उसकी आँखों में अपना तीनमंजिला मकान उतर आया|
“अपना कमरा तो अब खाली ही पड़ा होगा न?”
“तुझे क्या करना है…. खाली रहे या भरा? अब यही हमारा घर है| और देख तो, यहाँ कितनी लाटसाहबी है| किसी भी बात की कोई फिकर इ नइ| अपन दोनों बीमार पड़े, विवेक जब तक आया, तब तक तो इन लोगों ने डॉक्टर से दिखा भी दिया| एक दिन में हम ठीक भी हो गए|”
“हाँ, ठीक तो हो गए, मगर तुम्हें इतनी तीखी गरमी सूट कहाँ करती है! आए दिन ब्लड प्रेशर डराता रहता है| आज भी देखो तो शाम के पाँच बजने वाले हैं और धूप जलाने को तैयार बैठी है।”
“अब, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देख, अपने से अधिक बुड्ढे-बुड्ढे लोग पड़े हैं यहाँ| सब अच्छे परिवारों से हैं| वो दोनों चित्रकार पति-पत्नी! सोच,वे घर छोड़कर क्यों आए होंगे? उनका तो अपना मकान है और नीचे अम्मा जी का भी| उनका बेटा भी अफ़सर था| शादी की नहीं तो वह किसको दोष दे| एक वक़्त के बाद अपनी देखभाल नहीं होती तो घर की कौन करे! राशन जुटाओ,गैस बुक करो, आज पानी की किल्लत तो कल कोई और बखेरा| कम काम होते हैं क्या! अकेले हों या दुकेले, बूढ़े बूढ़े ही होते हैं| हर कोई प्रा’ जी जैसा लकी नइ होता|”
“क्या हम फिर कभी अपने घर नहीं जाएँगे?”
“नीलूss!”
अपने आवेश को दबाते हुए उसने हौले से कहा,”तुझे किसने रोका है? जब विवेक या नितेश साथ जाने को बोले तो चली जाना। अपने आप तो नहीं जा सकती ना!”
“तुम साथ नहीं चलोगे?”
“जब जाना होगा, तब की तब देखेंगे। अभी तुम परमिशन दो तो मैं ज़रा बाहर कॉरिडोर में दो चक्कर लगा आऊँ?” बात का रुख बदलते हुए उसने पत्नी से पूछा|
नीलू ने पति को देखा और उनकी आँखों में उतरे आवेश के लाल डोरे को गिनती हुई सिर हिलाकर हामी भर दी| वह जानती थी, इंदर को गुस्सा नहीं आता| आता है तो उसे दबाने की कोशिश में उसके दिमाग की नसें तन जाती हैं| हर समय कुछ सोचता रहता है, मगर जाहिर नहीं होने देता| घर की बात शुरू होते ही बात बदल देता है|
गरम हवा के थपेड़ों से घिरा वह कुछ देर ठिठका खड़ा रहा। उसका जी चाहा, वापस कमरे में लौट चलें मगर अभी, इस वक़्त अकेले रहने की इच्छा ने ज़ोर मारा तो उसने निगाहें दौड़ाईं। सबके दरवाज़े बंद पड़े थे मानो महीनों से खुले ही न हों, फिर अपने कमरे के दरवाज़े के भीतर नज़र घुमाते हुए दरवाज़ा अच्छी तरह सटा दिया।
कमरे से दो क़दम आगे निकलकर इंदर ज़ोर-ज़ोर साँस लेने लगा| घर की बातें, बेटों की आदतें, सरला की रुखाई, अपमान भरे शब्द -– सब जुड़-जुड़कर सुरसा का मुँह बन जाते और उसे निगलने लगते| इस बीच अक्सर उसे अपनी साँसें बोझिल लगने लगी थीं|
‘दिमाग की नसें तनी हुई हैं| सर फटा जा रहा है| कैसे समझाऊँ उसे कि मुझे नहीं जाना, कभी नहीं जाना उस दरवाज़े, जहाँ से निकल आया हूँ| उसे जाना हो तो जाए, मैं रोकूँगा भी नहीं, मगर मैं … नहीं मैं …जीते जी कभी नहीं|’
उसने पैरों की गति बढ़ा दी…..

सम्पर्क – dr.artismit@gmail.com